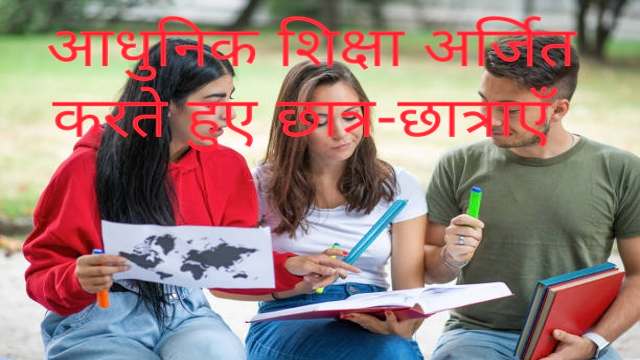Review of Education Objectives 2025
1.शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Education Objectives 2025),भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Objectives of Education in India 2025):
- शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Education Objectives 2025) से आशय है कि क्या वाकई में शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए वे वर्तमान शिक्षा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं।यदि शिक्षा के उद्देश्य मौजूद है तो क्या वह प्राप्त हो रहे हैं अथवा हम भटक तो नहीं गए हैं।
- आपको यह जानकारी रोचक व ज्ञानवर्धक लगे तो अपने मित्रों के साथ इस गणित के आर्टिकल को शेयर करें।यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो वेबसाइट को फॉलो करें और ईमेल सब्सक्रिप्शन को भी फॉलो करें।जिससे नए आर्टिकल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।यदि आर्टिकल पसन्द आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाईक करें जिससे वे भी लाभ उठाए।आपकी कोई समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Also Read This Article:Indian Education Should be Progressive
2.शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य (The Real Purpose of Education):
- किसी भी राष्ट्र के आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक एवं वैज्ञानिक विकास की आधारशिला उस राष्ट्र की श्रेष्ठ युवा पीढ़ी है।श्रेष्ठ युवा पीढ़ी से आशय ऐसी युवा शक्ति से है जो सभ्य,सुसंस्कृत,योग्य,अनुशासित,कर्त्तव्यनिष्ठ,नैतिक व चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण हो।ये सभी गुण युवाओं में शिक्षा द्वारा आते हैं।शिक्षा जहां एक ओर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर समाज तथा राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक एवं युवा शक्ति तैयार करती हैं,वहीं दूसरी ओर,यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है।शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा करना है जो उसे जीवन भर मार्गदर्शन कराती है और भटकने नहीं देती।शिक्षा एक ऐसा प्रकाश-स्तंभ है जो व्यक्ति को अंधकारों से मुक्त कर उसका सर्वांगीण विकास करता है।
- भारतीय संस्कृति विश्व की विशिष्टतम संस्कृतियों में एक अलग पहचान रखने वाली संस्कृति है।आज भी पश्चिमी राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति गौरव एवं सम्मान की प्रतीक है।यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति को जन्म दिया।प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित थी।उस काल में आश्रमों में प्रतिष्ठित आचार्यों के संरक्षण में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी,जिसमें तत्त्व व आत्मज्ञान के साथ कला,शिल्प,शस्त्र,नीति आदि चौदह विद्याएं सीखने का सुअवसर प्राप्त होता था।उस समय शिक्षा का मूल आधार मात्र रोजगार प्राप्त करना ना होकर आध्यात्मिक,नैतिक व सांस्कृतिक उत्थान था।संपूर्ण ज्ञान मौखिक आधार पर दिया जाता था।
- प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा हेतु तक्षशिला,नालंदा,विक्रमशिला व वल्लभी आदि संगठित संस्थाएं थीं।शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की प्राचीन परंपरा ने सामाजिक,नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की है,जिन्हें मानव समाज कभी विस्मृत नहीं कर सकेगा।मैक्समूलर ने कहा था,”जो जाति अपने अतीत पर,अपने साहित्य और इतिहास पर गर्व अनुभव नहीं कर सकती है,वह अपनी राष्ट्रीय चरित्र का मुख्य आधार खो देती है।” “शिक्षा का अर्थ है-सांस्कृतिक मूल्यों के अनेक लाभ पाने के लिए आवश्यक सुप्त शक्तियों के उद्दीप्त करने वाली मानसिक प्रक्रिया।” अर्थात् इसका प्रमुख उद्देश्य संस्कृति में निहित जीवन मूल्यों के अनुकूल आचरण की समझ उत्पन्न करना है,जिससे उसके समस्त लाभ प्राप्त किये जा सकें।हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है,जिसके द्वारा चरित्र-निर्माण होता है,मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है,बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।वास्तविक में शिक्षा का यही अभिप्राय ग्रहण किया जाना चाहिए।
- राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों का मूर्तरूप ही राजनीति होती है।ये आधारभूत सिद्धांत वहां की संस्कृति ही निर्धारित करती है और वही संस्कृति बीजरूप में शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचती हैं।
- प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों एवं गुरुकुलों में अपने मूल प्राकृतिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहकर उनका यथोचित रूपेण संपादन करती रही क्योंकि तब शिक्षा राजकाज का अंग नहीं थी।परंतु जैसे ही आधुनिक राजनीति की बदली हुई परिभाषा के विषयक्षेत्र में शिक्षा को भी समेट लिया गया वैसे ही वह अपने मूल उद्देश्य से भटक गई।शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में गंदी राजनीति की घुसपैठ समग्रतः अंग्रेजों के काल में हुई,उन्होंने शिक्षा को अपने निहित स्वार्थ-साधन की चिरकालिक सहायिका बना लिया।
3.शिक्षा में गंदी राजनीति की घुसपैठ (Intrusion of dirty politics into education):
- उदार शिक्षा के नाम पर भारत में उन्होंने (अंग्रेजों) यहां की दिव्य प्राचीन संस्कृति को समूल नष्ट करने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा।उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों के हृदय को उन्हीं की संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना से भर देना था तथा उनके आचार-विचारों,मान्यताओं के प्रति निष्ठाहीन बनाना था,ताकि वे शरीर से भारतीय परंतु मस्तिष्क से “पाश्चात्यों के मानस-पुत्र” बन सकें।धूर्त अंग्रेज अपने इस नापाक उद्देश्य में बड़ी सरलता से सफलीभूत हुए।आज प्रशासन में उच्च पदाधिकारी से लेकर साधारण क्लर्क तक में भी वर्णसंकर संस्कृति का तांडव दीख पड़ता है।यह शिक्षा में राजनीति की घुसपैठ का अत्यंत दुःखद परिणाम हुआ।
- राजनीति में प्रथम तो ज्ञान की शिक्षा से अलग कर दिया फिर शिक्षा और साक्षरता के बीच नया समीकरण उपस्थित किया।”साक्षरता का विरोध तो कोई भी कदापि नहीं करेगा,किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा कोई और ही वस्तु है जो कि सहज साक्षरता से बहुत अलग होती है।वस्तुतः साक्षरता से अज्ञान का प्रसार होता है।केवल लिखना-पढ़ना जान लेने से अज्ञान तो दूर नहीं हो जाता।फिर भी हमारे राजनीतिज्ञ अब तक यही कहते रहे हैं कि साक्षरता के प्रसार से देश की भोली-भाली जनता ज्ञानी बनकर लोकतंत्र को सफल बनाएगी।”
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश के राजनीतिज्ञ अंग्रेजों के आभारी हुए और उन्हीं के नक्शे-कदम पर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की।उनके प्रोत्साहन और गलत शिक्षा के फलस्वरूप नामधारी लेखक व्यक्ति-विकास के लिए अपने मूर्ख भाइयों को “प्रेयस” को ही “श्रेयस” मान लेने का प्रचार करने लगे।विदग्ध कहे जाने वाले साहित्य का मुख्य-स्वर ठीक यही है।इस भ्रान्त धारणा का अवश्यंभावी परिणाम यह हुआ कि मानव के विचारों एवं आचारों का कोई तात्विक आधार नहीं रह गया।नैतिकता और नैतिक-शिक्षा की किसी ने कोई परवाह ही नहीं की और वह शनैः-शनैः उत्तरोत्तर अधःपतित होती गयी।
- आज यह बात सर्वसम्मत हो चुकी है कि नैतिक शिक्षा समाज की सुस्थिरता के लिए नितांत आवश्यक है,किंतु यदि नीति का कोई तात्विक आधार न हो और वह व्यक्ति-संबंध-हीन रहे तो उसकी कितनी भी महत्ता गायी जाए,तथा शिक्षा का कितना भी आडंबर रचा जाय,फिर भी वह हृदय में बद्धमूल नहीं हो सकती।प्रवर्तक मन को यह अगोचर ही रहती है।इस तरह सुविधाओं की वर्षा होने पर भी अंतःकरण उससे कमल-पत्र की भांति अविरत ही रहता है और अंततः समाज को आगे बढ़ाने के लिए भय या लोभ का आश्रय लेना पड़ता है।शीघ्र ही सारा समाज मानव-पशुओं के विशाल जंगल के रूप में परिणत हो जाता है-इतना ही नहीं,यह मानव-पशु हिंस्र वन्य पशुओं से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लेता है।
- राजनीति की तरह आज शिक्षा का रूप भी प्रचारात्मक हो गया है।राजनीति भी राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों का मूर्तरूप अब नहीं रही-आजकल तो राष्ट्रों में राजनीति के अनुकूल सिद्धांत गढ़े जाते हैं और उन्हीं की खुराक (Dose) शिक्षा के रूप में छात्रों को पिलाई जाती है।किसी भी राष्ट्र में आजकल के राष्ट्राधिकारी राष्ट्र का दर्शन और शिक्षा दोनों को राजनीति के अनुकूल बनाये रखने की दृष्टि से नियंत्रित करते हैं।
- सामाजिक शिक्षा के अंतर में ज्ञान प्रसार की अपेक्षा राजनीति के ढांचे में ढालने योग्य विचार रखने वाले अनुयायी पैदा करने का पाप अधिक समाया रहता है।ऐसी शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य यह होता है कि सच्चे ज्ञान को एक ओर रखकर छात्रों के हृदय को ही अपेक्षित ढंग से गढ़ा जावे।
4.शिक्षा में राजनीति का दुष्परिणाम (Consequences of Politics in Education):
- भारत के संदर्भ में,शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति की घुसपैठ और दुराग्रही नीति-निर्धारण या पद-प्रच्छालन से जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उनमें प्रथम तो एंग्लोअमेरिकन शिक्षा के अंधानुकरण से युवकों में नैतिक अधःपतन और गैर जिम्मेदारी बढ़ी।दूसरे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने की जल्दबाजी और उतावली ने माध्यमिक शिक्षा की जड़ों पर आघात किया और उसका स्तर बहुत गिर गया।तीसरे,अंग्रेजों की कुटिल-नीति की बुनियाद पर खड़ी की गयी शिक्षा पद्धति ने छात्रों में अपनी परंपरा तथा आचार-विचार के प्रति अनादर और तिरस्कार पैदा कर दिया।जीवन-विषयक कोई भी गंभीर चिंतन ना होने से,दर्शन न होने से,इसमें निष्ठा निर्माण की सामर्थ्य ही नहीं रही,फलतः साक्षर बनाकर ज्ञान का आडम्बर रचाये जाते हैं और व्यवहार में प्रबल पाशविक-वृत्ति का ही परिचय देते हैं।चौथे,राजनीति की तरह शिक्षा का रूप भी प्रचारात्मक हो गया है।आज सामाजिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मौलिक निष्ठाओं का उन्मूलन कर ध्येयहीन जीवन बिताना ही है।
- इस तरह राजनीति ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया और उसे अपने लक्ष्य से,उद्देश्य से च्युत करके पथभ्रष्ट किया।आज शिक्षा बुद्धि का विलास मात्र रह गई।शिक्षा के नाम पर जो धीमा-विष छात्रों के मस्तिष्क में धीरे-धीरे घोला गया,वही एकमेव रूप में अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा है और सर्वत्र नैतिक तथा चारित्रिक अवमूल्यन एवं भ्रष्टाचार का अभूतपूर्व उत्कर्ष दिखाई पड़ रहा है।राजनीति ने वर्तमान शिक्षा से हृदय तत्व और आत्मतत्व को बड़ी चतुराई से अलग करके मात्र बुद्धितत्व को ही रहने दिया है-वह भी विकृत रूप में।तथाकथित शिक्षित समुदाय अपनी आदर्श परंपराओं को तोड़ने में ही शिक्षा की सार्थकता देखते हैं।किसी प्रेरक-आदर्श के अभाव में शिक्षा एकांकी होकर सहज कागजी रह गई है-आत्मोन्नति में उसकी किंचित भी उपयोगिता नहीं रही।
- शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न अंतर्राष्ट्रीय एकता,वरन व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि उसमें बुद्धि से भी महत्त्वपूर्ण कोई चीज है,जिसे आत्मा कह सकते हैं।
- परंतु आज की लक्ष्यहीन डिग्री-मूलक शिक्षा में यही महत्त्वपूर्ण बात छोड़ दी गई है,इसीलिए पढ़ाई खत्म करके निकला हुआ छात्र स्वयं को एक चौराहे पर खड़ा पाता है-दिग्भ्रान्त और अनिश्चय की स्थिति में वह जीविका के लिए दर-दर की ठोकरें खाकर अपनी मानसिक दासता से साक्षात्कार करता है,तथा कहीं की क्लर्की आ जाने में ही जीवन की चरम सफलता समझने की नियति का शिकार होता है।मानसिक रूप से पंगु और शारीरिक रूप से अकर्मण्य तथा विलासप्रिय क्लीव बनाने वाली इस शिक्षा से देश में पुच्छवृषाणहीन मानव-पशुओं की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और उनके भार-स्वरूप अनुत्पादक अस्तित्व का बोझ अपढ़ किंतु मेहनतकश कृषक मजदूरों को ढोना पड़ रहा है।
- शिक्षा में राजनीति की अनावश्यक दखलंदाजी के इस भयंकर दुष्परिणाम से हमारे राजनीतिज्ञ अनभिज्ञ नहीं हैं,परंतु उनके अपने निहित स्वार्थ हैं जिनकी वजह से वे इसी गलित व्यवस्था को किसी न किसी तरह बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं।अंतत वे भी उसी मानसिकता की उपज हैं जिसमे राष्ट्र,संस्कृति,आत्मा,त्याग,सेवाधर्म आदि शब्द अपना अर्थ-संवेदन खोकर ‘एकांतिक स्वार्थ’ की बेदी पर होम हो जाते हैं।’मानव कल्याण’,’देश कल्याण’ की पूत-भावना ‘स्वकल्याण’ में तिरोहित हो जाती है।कहीं कभी इसी अव्यवस्था की कसक का स्वर उठता है तो सुधार के नाम पर गलदश्रु बहाएं जाते हैं,कभी न समाप्त होने वाला भाषणों का सिलसिला चल पड़ता है परंतु इस विषय पर कोई गंभीर चिंतन मनन नहीं किया जाता बल्कि सड़े दिमागों की सनक पर अनेकशः विकृत प्रयोग होते हैं जिनसे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होती है।सरकारी नीति के अनुरूप समाज का अयोग्य और नकारा समझा जाने वाला वर्ग बुनियादी-शिक्षक की नौकरी अनचाहे स्वीकार करके अपना नकारापन छात्रों में बाँटकर उसी की रोटी तोड़ता है।पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ कीचड़ की गिलगिजी नींव पर अपना जीवन-महल खड़ा करने के लिए भाग्य भरोसे छोड़ दिए जाते हैं।
- वर्तमान लक्ष्यहीन,दिशाहीन तथा आदर्शहीन शिक्षा आज की कुत्सित राजनीति की देन है,और हम हैं कि उसे अंगीकार किए हुए विकल्पहीन,आत्मघात के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं।
5.शिक्षा के उद्देश्यों का निष्कर्ष (Conclusion of the objectives of education):
- उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में,आवश्यकता इस बात की है कि नैतिक और चारित्रिक अवमूल्यन के इस अबाध,उद्याम वेग को प्रयत्नपूर्वक रोककर ढहती हुई सांस्कृतिक आस्था को,आदर्श को,और भारत के भविष्य को बचाया जावे।शिक्षा को राजनीतिक दलदल से उबारकर,भारतीय संस्कृति के नैतिक आदर्श पर आधारित किया जावे।राजनीति परस्त,राजनीति तय करते रहें शिक्षा नीति में दखल न दें ताकि शिक्षा अपने गत-उद्देश्यों को पुनः साधकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके।शिक्षा संस्थान राजनीति का अखाड़ा न बनकर पवित्र ज्ञान मंदिर बने,और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सरो-सामान जुटाने में सभी नीतिज्ञ मनसा-वाचा-कर्मणा सहयोग देकर आने वाले कल का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करें।
- हालांकि यह कार्य है तो कठिन क्योंकि शिक्षा में जिस तरह,राजनीति की घुसपैठ हो गई है और राजनेताओं को जिस प्रकार इसका चस्का लग गया है उससे निकल पाना कठिन है।परंतु शिक्षा के शुद्धिकरण,अपने परम वैभव पर पहुंचाने का और कोई विकल्प भी नजर नहीं आता है।सामान्य जनमानस भी लोकलुभावन सुविधाओं का इतना आदी हो गया है कि वह हर क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं का मोहताज हो गया है।वह हर किसी क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं की आकांक्षा रखता है।अपनी मेहनत,अपने परिश्रम पर विश्वास न करके यह प्रवृत्ति उसे परमुखापेक्षी बना देती है।उसकी कर्मठता को लकवा मार गया है।वह मिल रही सुख-सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहता।सरकारी रेवड़ी के इंतजार में ही अपनी नैया को पार लगाने के सपने देखता है।
- राजनीतिज्ञ उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसके लिए लोकलुभावन वायदे करते हैं।जबकि शिक्षा के क्षेत्र में पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए पूरे तंत्र की सर्जरी करनी होगी तभी शिक्षा तंत्र दुरुस्त हो सकता है,शिक्षा क्षेत्र की कायापलट हो सकती है।शिक्षा क्षेत्र में उपर्युक्त बदलाव के लिए बहुत बड़े नैतिक बल,दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता है।यदि ऐसा किया जा सके तो शिक्षा में घुसपैठ हो चुकी गंदी राजनीति को निकाला जा सकता है।राष्ट्र के नैतिक चरित्र को उज्ज्वल करने के लिए शिक्षा पहले पायदान का काम करती है।शिक्षा में बदलाव के लिए ऐसे कठोर कदमों को उठाने की जरूरत है।जनमानस को अपने लोभ का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।तभी चरित्रवान युवा पीढ़ी तैयार हो सकती है और यह राष्ट्र पुनः विश्वगुरु के पद पर सुशोभित हो सकता है।भारत के पुराने वैभव को लौटाने के लिए दो आधार स्तंभ हैं:पहला प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत कृषि,उद्योग तथा इनसे संबद्ध घटक आते हैं;दूसरा मानवीय संसाधन या सांस्कृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत सर्वांगीण मानव विकास अर्थात् राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावनाओं का विकास होता है।प्रथम का उत्तरदायित्व उद्योगपतियों,कृषकों एवं शासकों का है जबकि द्वितीय उत्तरदायित्व शिक्षकों एवं शिक्षा नीति पर है।
- उपर्युक्त आर्टिकल में शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Education Objectives 2025),भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Objectives of Education in India 2025) के बारे में बताया गया है।
Also Read This Article:Criticism of Indian Education System
6.छात्र का डर (हास्य-व्यंग्य) (Student’s Fear) (Humour-Satire):
- शिक्षक (छात्र से):इस तरह क्यों डर रहे हो?
- छात्र:दरअसल मैं कोचिंग पहली बार कर रहा हूं।
- शिक्षक:तो इसमें डरने की क्या बात है,मैं भी पहली बार कोचिंग करा रहा हूं।
- छात्रःसर,यह जान चुका हूं;तभी तो डर लग रहा है कि फेल न हो जाऊं।
7.शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Frequently Asked Questions Related to Review of Education Objectives 2025),भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Objectives of Education in India 2025) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न:1.छात्रों में नैतिक पतन को कैसे रोकें? (How to prevent the moral decay of students?):
उत्तर:छात्रों में गिरते हुए नैतिक मूल्यों की रोकथाम हेतु शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है।
प्रश्न:2.छात्रों में रचनात्मकता का विकास कैसे हो? (How to develop creativity in students?):
उत्तर:विद्यालय एवं महाविद्यालयों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएं,जिससे छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व रचनात्मकता का विकास हो।
प्रश्न:3.छात्रों में कुंठा को कैसे रोकें? (How to Prevent Frustration in Students?):
उत्तर:वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप ऐसा है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात छात्र को रोजगार ढूंढने में कठिनाई होती है,फलतः उसमें कुण्ठा उत्पन्न होती है अतः शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए।
प्रश्न:3.छात्रों में कुंठा को कैसे रोकें? (How to Prevent Frustration in Students?):
उत्तर:वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप ऐसा है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात छात्र को रोजगार ढूंढने में कठिनाई होती है,फलतः उसमें कुण्ठा उत्पन्न होती है अतः शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए।
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Education Objectives 2025),भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा 2025 (Review of Objectives of Education in India 2025) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| No. | Social Media | Url |
|---|---|---|
| 1. | click here | |
| 2. | you tube | click here |
| 3. | click here | |
| 4. | click here | |
| 5. | Facebook Page | click here |
| 6. | click here | |
| 7. | click here |
Related Posts
About Author
Satyam
About my self I am owner of Mathematics Satyam website.I am satya narain kumawat from manoharpur district-jaipur (Rajasthan) India pin code-303104.My qualification -B.SC. B.ed. I have read about m.sc. books,psychology,philosophy,spiritual, vedic,religious,yoga,health and different many knowledgeable books.I have about 15 years teaching experience upto M.sc. ,M.com.,English and science.