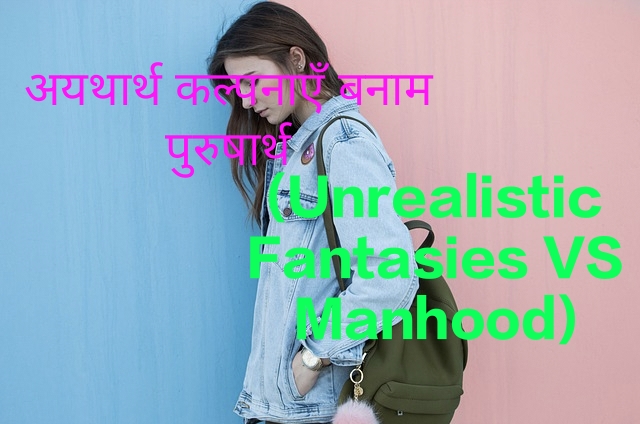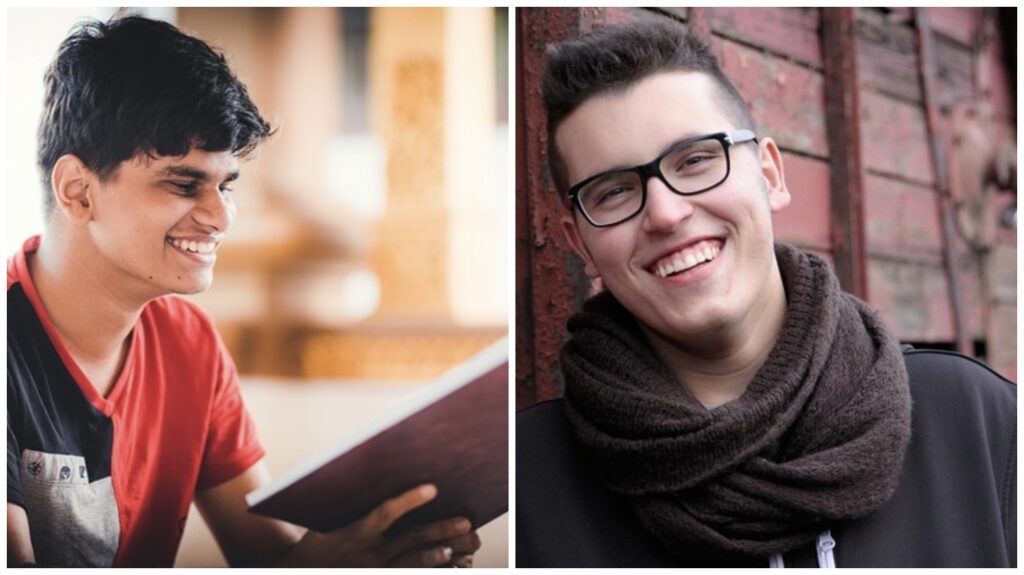Unrealistic Fantasies VS Manhood
Contents
hide
1.अयथार्थ कल्पनाएँ बनाम पुरुषार्थ (Unrealistic Fantasies VS Manhood),कल्पनाओं का जाल बनाम पुरुषार्थ (Fantasy VS Manliness):
- अयथार्थ कल्पनाएँ बनाम पुरुषार्थ (Unrealistic Fantasies VS Manhood) के आधार पर कल्पनाओं को साकार करने का पुरुषार्थ कर सकेंगे।केवल कल्पनाओं में खोए रहने या अव्यावहारिक कल्पनाएँ करते रहने से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
- आपको यह जानकारी रोचक व ज्ञानवर्धक लगे तो अपने मित्रों के साथ इस गणित के आर्टिकल को शेयर करें।यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो वेबसाइट को फॉलो करें और ईमेल सब्सक्रिप्शन को भी फॉलो करें।जिससे नए आर्टिकल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।यदि आर्टिकल पसन्द आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाईक करें जिससे वे भी लाभ उठाए।आपकी कोई समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Also Read This Article:विधेयात्मक कल्पना कैसे करें?
2.कल्पनाओं का जाल (Trap of fantasies):
- काश! वो मिलते तो हमारी जिंदगी ऐसी होती।काश! उनके होने से हम ऐसा करते।ये तमाम कल्पनाएं-परिकल्पनाएँ हमें सान्त्वना देती हैं कि उनके होने से हम कुछ अच्छा कर पाते।वे कौन हैं,जिनको हम चाहते हैं? उनकी कैसी सहायता जो हमें चाहिए? ऐसा तब होता है,जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं,उनके प्रभाव-परिणाम से प्रभावित होते हैं या किसी महान गणितज्ञ या वैज्ञानिक का उत्तम जीवन चरित्र पढ़ते हैं।बात बड़ी कड़वी है और यथार्थ भी कि हम अपनी परिकल्पनाओं के आदर्श के मिलने के बावजूद ऐसे ही होते जैसे आज हैं।कहीं कोई बदलाव नहीं होता,बल्कि एक अपराधबोध और घेर लेता है कि उनके जैसे व्यक्तित्व के साथ रहकर भी हम कुछ नहीं कर पाए।
- ‘काश’! कहकर जो एक गहरी निःश्वास छोड़ते हैं,यह हमारी सामर्थ्य अथवा जज्बा का पर्याय नहीं है,वरन अक्षमता,अकर्मण्यता का परिचायक है।जिसे हम दूसरों पर आरोपित करते हैं और हम संतोष की सांस लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हो सके या कर सके,इसलिए कि हमें कोई अच्छा गणितज्ञ,वैज्ञानिक,काउंसलर,पथप्रदर्शक एवं मार्गदर्शक नहीं मिल सका।परंतु इस परोक्ष दोषारोपण में हम यह भूल जाते हैं कि यदि वे जिन्हें हम चाहते हैं,होते तो उनसे क्या लाभ ले सकते।वस्तुतः सामान्यजन स्वार्थ और अहंकार का पुतला होता है।स्वार्थ सधते ही भाग जाता है और अहम की पुष्टि होने पर फूलकर कुप्पा बन जाता है।कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता।
- हम जिस गणितज्ञ,वैज्ञानिक,संत,महामानव की या आदर्श की कल्पना करते हैं,उसके होने से क्या लाभ होता? इतिहास इस प्रश्न का जवाब देता है।यदि हमारा आदर्श संपन्न और समृद्ध होता तो हम उससे बिना परिश्रम से वह सब कुछ पा जाना चाहते हैं,जो कि उसके पास होता और जिसे उसने कठिन परिश्रम एवं लगन से अर्जित किया है।यदि वह आदर्श विद्वान,ज्ञानी एवं प्रसिद्ध व्यक्ति होता तो हम चाहते कि वह अपना सारा ज्ञान हमें अनायास उँड़ेल दे और हमें भी अपने समान अपने से ज्यादा विख्यात कर दे।यदि आदर्श वैज्ञानिक होता तो वह अपनी तमाम खोज एवं अनुसंधान को हमारे नाम कर देता और हम बदले में उससे चाहते कि वह हमारा सहायक बने और हमारे मनोनुकूल ही सब कुछ करे।
- यदि हमारे आदर्श की कल्पना आध्यात्मिक व्यक्ति के मिलने की है तो स्थिति और भी बदतर होती।कहते-लिखते शब्द सकुचाते हैं,शरमाते हैं,परंतु कड़ुवे यथार्थ के बयान के कहना पड़ता है कि हम अच्छे आदर्श को कैद कर और भी अकर्मण्य और असंवेदनशील हो जाते।अध्यात्म सृष्टि के गहन अस्तित्व का ज्ञान एवं तकनीक है।इससे हम सृष्टि के गोपनीय रहस्य से अवगत भी हो सकते हैं और उसे पाने की तकनीक भी जान सकते हैं।इससे तमाम ऋद्धियाँ-सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।हवा में उड़ना,धनवर्षा,पारस के स्पर्श से लोहे को सोना बनाना,व्यक्ति के गोपनीय रहस्य को जान लेना,ऐसे तमाम लौकिक एवं अलौकिक कार्य अध्यात्म विद्या से संभव हो सकते हैं।इससे भी बड़ा कार्य कि मानवीय चेतना में आमूलचूल परिवर्तन,रूपांतरण भी इस विद्या से संभव है।
3.अद्भुत और चमत्कारिक कार्य (Amazing and wondrous work):
- अध्यात्म की ऐसी चमत्कारी एवं अद्भुत सिद्धि यदि किसी के पास हो और वह आध्यात्मिक पुरुष हमें मिल जाए तो हमारी अपरिपक्व मानसिकता उससे क्या चाहेगी? हम चाहेंगे कि वह हमारी मनोकामना पूरी करने की मशीन बन जाए,हम जैसे कहें वह करता जाए।हमारी दादी का स्वास्थ्य ठीक कर दे।व्यापार या नौकरी में घाटा चल रहा हो तो वह लाभ करा दे।घर में सेवा करने के लिए नौकरानी देरी में आ रही हो जल्दी बुला दे।अर्थात् हर छोटा-बड़ा कार्य हम उससे कराना चाहेंगे।औरों को प्रसन्नता एवं सुख देने के लिए वह सब कर भी देता है।उसके इस अनुदान देने के अनुपात में हमारी लोभ-लालसा भी बढ़ती जाती है और अंततः हम उसे ऐसा अलादीन के चिराग से निकला जिन्न बना देते जिससे वह जैसा,जब हम चाहें पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता।
- सामान्यजन की सामान्यतः यही अवधारणा होती है।बहुत से ऐसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुए हैं जो अपने विषय के ज्ञाता तो थे ही साथ ही अध्यात्म विद्या से संपन्न भी थे।अध्यात्म विद्या के आधार पर वे चकित कर देने वाली खोजें कर सके थे।इस रहस्य का पता जब आम छात्र-छात्रा को लगता है तो उनकी कामना होती है कि भगवान से उन्हें धन-दौलत,संसार के ऐश्वर्य मांगने चाहिए परंतु ऐसी मंशा उन महान गणितज्ञों एवं वैज्ञानिकों को व्यथित कर देती है।वस्तुतः इस संसार में कौन भगवान को चाहता है? अर्थात् ऐसे बहुत कम लोग हैं।कौन अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहता है? सभी उसके भौतिक ऐश्वर्य का लाभ लेना चाहते हैं।उसे कोई नहीं चाहता।
- आदर्श का मिलना एक महान घटना है,परंतु आदर्श के प्रति समर्पण का भाव एक अत्यंत दुर्लभ घटना है।देने के लिए,अनुदान लुटाने के लिए गुरु सदैव तत्पर होता है,लेने वालों की कमी होती है।गुरु तो सहज ही बादलों जैसे बरस पड़ता है,परंतु शिष्यत्व का समर्पण चुक जाता है।हम मांगते तो हैं,परंतु भिखारी के समान।लोभ ललचाता है,वासना सताती है,क्रोध का वेग झेला नहीं जाता,आसक्ति परेशान करती है और अगर ऐसे में कोई मिल जाए तो उससे इंद्रिय सुखों के लिए हम ऐसी चीजों की मांग करते हैं कि देने वाला भी शर्मसार हो जाता है। ऐसे में यदि हम कहते हैं कि काश! कोई मिलता,अगर मिलता भी तो कुछ नहीं होता,हम वहीं के वहीं खड़े मिलते,जहां वर्तमान में हैं।
- पुरुषार्थी को कोई ना मिले तो वह भी पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ता।ऐसी अनेक प्रतिभाएं पैदा हुई हैं जिन्हें कोई सुयोग्य मार्गदर्शक नहीं मिला।लेकिन उनकी लगन और निष्ठा ही थी कि अंततः वे शिखर पर जा विराजे।हालाँकी शीर्ष पर पहुंचने के लिए अनेक ठोकरे खानी पड़ती है,बहुत कड़ुवे अनुभव होते हैं,संघर्ष करना पड़ता है तब कहीं जाकर उन्हें अपना लक्ष्य मिल पाता है।इसके लिए उन्हें बहुत कीमत चुकानी पड़ती है।लेकिन ऐसी प्रतिभाएं ऐसी मिट्टी की बनी होती हैं कि उनका त्याग और पुरुषार्थ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं।कहीं भी,कभी भी वे अपने को कमजोर नहीं पड़ने देते।संघर्ष की भट्टी में तपकर निखरते हैं।उनके अंदर धधकती प्रचंड भगवद् निष्ठा ही उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। ऐसे अनगिनत ज्वलंत उदाहरण हैं जो बताते हैं कि त्याग और बलिदानी मानसिकता अपने इष्ट और लक्ष्य से लौकिक कामना नहीं करती,बल्कि वह तो मांगने के बदले स्वयं को लुटा देती है,विलय कर देती है।
- सागर में नदी अपने को मिटा देती है।उसे मिटा देने में ही पाने का अपार आनंद समाया हुआ है।नदी सागर से मिलने से पूर्ण विराट की कामना करती तो भला यह कैसे होता? बूंद की लघुता समुद्र की विभुता में चरम उपलब्धि पाती है।मांगना ही है तो क्यों न ज्ञान,भक्ति,तप,वैराग्य मांगा जाए,जबकि देने वाला देने के लिए द्वार पर खड़ा है।होना और बनना है तो क्यों न आकाश जैसा व्यापक बन जाएँ और काश! हम ऐसे हों कि कसक और पीड़ा को मानवता की पीड़ा से तदाकार कर लें,फिर तो कोई मिले या ना मिलें,लक्ष्य के प्रति बढ़ते कदम न कभी रुकेंगे और ठहरेंगे।यही एकनिष्ठ भाव किसी मार्गदर्शक सत्ता से अवश्य जोड़ेगा।अतः हमें सतत बिना रुके,बिना किसी से अपेक्षा किये अपने श्रेष्ठ कर्म में विरत रहना चाहिए।
4.मस्तिष्क कल्पनाएँ करता रहता है (The brain keeps imagining):
- मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब व्यक्ति कल्पनाएँ नहीं कर रहा होता है,तब भी वह कल्पनाएं करता रहता है।प्रथम दृष्टि में कथन कुछ पहेली-सा प्रतीत होता है कि जब हम स्वयं कल्पनाएँ ही नहीं कर रहे होते हैं तो फिर मस्तिष्क कैसे कल्पनाएं करेगा! बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है;क्योंकि मस्तिष्क की क्रिया का भी अपना महत्त्व और स्थान है।यह सत्य है कि मनुष्य जब कल्पनाएं करता है तो साथ-साथ मस्तिष्क भी कल्पनाएं करता है या दूसरे शब्दों में कहे तो यह कहना पड़ेगा कि वह मस्तिष्क के माध्यम से ही कल्पनाएं करता है,किंतु असत्य यह भी नहीं है कि जब मनुष्य कल्पना नहीं करता है,तब मस्तिष्क शांत नहीं बैठा रहता,कुछ ना कुछ ताने-बाने बुनता रहता है।
- अब यह कोई छिपी बात नहीं रही कि स्थूल मस्तिष्क अथवा चेतन मस्तिष्क के अतिरिक्त उसकी अन्य कई परतें भी हैं,जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में चेतन,अचेतन,अवचेतन और सुपरचेतन के नाम से जाना जाता है।मनोविज्ञानवेत्ता जब यह कहते हैं कि मनुष्य जब शांत-एकांत में पड़ा रहता है,तब भी उसका मस्तिष्क सक्रिय रहता है तो इससे उनका इशारा चेतन मस्तिष्क से नहीं,वरन उसकी अन्य परतों की ओर होता है।
- प्रयोगों के दौरान देखा गया है कि कई बार जो संदेश चेतन मस्तिष्क को दिए जाते हैं,उन्हें वह अनावश्यक और अनुपयोगी समझकर छोड़ देता है,पर उन्हीं निरर्थक लगनेवाले संकेतों से मस्तिष्क की सूक्ष्म परतो में हलचल मच जाती है और उसके अनुरूप वह कार्य करना आरंभ कर देता है।इसे यदि सूक्ष्म मस्तिष्क का कल्पना करना कहा जाए तो अनुपयुक्त ही क्या है! यद्यपि स्थूल चिंतन हमारा रुका हुआ है।
- इसी सिद्धांत के आधार पर अनेकानेक प्रयोग कर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि चेतन मस्तिष्क को उपयुक्त संदेश दिया जाए तो अवचेतन मस्तिष्क में घुसी विकृतियों,व्यसनों,कुंठाओं और रोगों को निकाल बाहर किया जा सकता है।इसी को ऑटोसजेशन,हेट्रोसजेशन के माध्यम से क्रियान्वित भी किया जा रहा है एवं इसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे हैं।जब हम सोते हैं अथवा जागते हुए सुषुप्ति जैसी स्थिति में पड़े रहते हैं,तब भी मन-मस्तिष्क शांत बना नहीं रहता,अपितु कल्पनाओं के जाल में उलझा रहता है और उसे जो काम की बात लगती है,उसे वह संरक्षित रखकर शेष को छोड़ देता है।अर्थात् उसके अनुसार मस्तिष्क इस दौरान सूचनाओं की छँटनी में व्यस्त रहता है।
- मनोविज्ञान की इस विधा द्वारा मनोविकारों को भी हटाया-मिटाया जा सकता है।यदि हम चेतन मस्तिष्क को बार-बार कोई सूचना दें तो देखा गया है कि अनेक प्रयासों के उपरान्त वह मस्तिष्क की सूक्ष्म परतों में धँस जाती है एवं वैसी ही क्रियाएँ और परिस्थितियाँ विनिर्मित करने लगती है,जैसा संदेश होता है।यद्यपि सूचनाएँ दिन में कुछ ही बार देनी पड़ती हैं,किंतु अवचेतन मस्तिष्क उस आधार पर अहिर्निश कार्य करने लगता है।सूक्ष्म मस्तिष्क की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर यदि यह कहा जाए कि तब हम कल्पनाएं नहीं करते हैं,तो भी मस्तिष्क कल्पनाएं करता रहता है,तो इसमें अत्युक्ति क्या है?
5.विद्यार्थी कल्पना और पुरुषार्थ में तालमेल करें (Students should combine imagination and effort):
- अब प्रश्न उठता है कि कल्पना और पुरुषार्थ में श्रेष्ठ कौनसा है क्योंकि कल्पनाओं,ज्ञान के बिना पुरुषार्थ (अध्ययन) करना व्यर्थ सिद्ध होता है।परंतु यह साधारण स्थिति की बात है।गहराई से देखने पर पुरुषार्थ (निष्काम कर्म) कल्पना,चिंतन,मनन,ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ होता हैं।क्योंकि कल्पनाओं,चिंतन-मनन की बातों को साकार करने का कार्य पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। पुरुषार्थ के बिना कल्पनाएं कोरी कल्पना ही रह जाती हैं,चिंतन,सोच-विचार की बातें बौद्धिक व्यायाम ही सिद्ध होती है।पुरुषार्थ के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि कौनसी कल्पनाएं सार्थक,व्यावहारिक व उपयोगी है जिनको साकार किया जा सकता है।जिन कल्पनाओं को साकार नहीं किया जा सकता है वे कल्पनाएँ निरर्थक,अव्यावहारिक होती हैं।
- उदाहरणार्थ आप यह कल्पनाएँ करें कि मैं पक्षी बन जाऊँ,साक्षर हुए बिना,पढ़े-लिखे बिना,अनपढ़ लड़का,योग्यता प्राप्त किए बिना छात्र-छात्रा यह कल्पना करने लगे कि वह आईएएस बन जाए।
- पुरुषार्थ के द्वारा ही कल्पनाओं की छँटनी होती है,जो कल्पनाएं निरर्थक व अव्यावहारिक हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए।अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह व्यावहारिक कल्पनाएँ करें,सार्थक कल्पनाएँ करें जिससे आप समय की बचत कर सकते है।सार्थक व व्यावहारिक कल्पनाओं के लिए मन-मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना एक दिन में संभव नहीं होता है।इसके लिए बुद्धि सात्विक होनी चाहिए,सद्ज्ञान का होना जरूरी है।क्योंकि सद्बुद्धि,प्रज्ञा के द्वारा ही कल्पनाओं की छँटनी की जा सकती है,विवेक के द्वारा अयथार्थ,अवास्तविक कल्पनाओं के ताने-बाने में उलझे रहने को रोका जा सकता है।
- अतः पुरुषार्थ के साथ-साथ विद्यार्थियों को ज्ञान,विद्या अर्जित करते रहना चाहिए।क्योंकि पुरुषार्थ को सही दिशा भी सद्ज्ञान,सद्बुद्धि,विवेक के द्वारा दिया जा सकता है।यह ठीक है कि पुरुषार्थ का महत्त्व कम नहीं हो जाता है।अपनी-अपनी जगह हर गुण का महत्त्व होता है।आप कर्म ही करते रहे,अध्ययन ही करते रहे,उस पर अमल न करें तो उस कर्म का क्या महत्त्व है? आप जो-जो अध्ययन कर रहे हैं उस पर विचार न करें कि कौन-कौनसी बातों का अध्ययन करना चाहिए,किन-किन बातों का अध्ययन नहीं करना चाहिए तो आप अनावश्यक,कूड़ा-करकट भी मस्तिष्क में भर लेंगे जिसकी आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है।ध्यान रहे यहाँ पुरुषार्थ से तात्पर्य है निष्काम कर्म।निष्काम कर्म की स्थिति तभी उपलब्ध होती है जब आप सद्ज्ञान,सद्बुद्धि को धारण करते हैं।
- आप कल्पनाशील नहीं होंगे तो नहीं-नई बातों का अध्ययन कैसे कर पाएंगे,अपने व्यक्तित्व को प्रभावी कैसे कर पाएंगे।यों साधारण कर्म (अध्ययन) की अपेक्षा ज्ञान (सद्ज्ञान) श्रेष्ठ होता है क्योंकि ज्ञान के बिना साधारण कर्म मूल्यवान,सार्थक और सफल नहीं हो सकता है।तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है अतः निष्काम कर्म (अध्ययन) करने की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न,पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।अभ्यास,ज्ञान प्राप्त करने,सार्थक व व्यावहारिक कल्पना करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है अर्थात् सबकुछ संभव है,अतः विद्यार्थी को सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर द्वारा अयथार्थ कल्पनाएँ बनाम पुरुषार्थ (Unrealistic Fantasies VS Manhood),कल्पनाओं का जाल बनाम पुरुषार्थ (Fantasy VS Manliness) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Also Read This Article:छात्र-छात्राओं में कल्पना शक्ति का विकास कैसे करें?
6.कल्पना में खोया हुआ (हास्य-व्यंग्य) (Lost in Fantasy) (Humour-Satire):
- एक छात्र कल्पना लोक में विचरण कर रहा था।दूसरे छात्र ने उसे इस स्थिति में देखकर झिंझोड़ा और कहा,कहां खोए हुए थे।
- पहला छात्रःमन में ऐसी कल्पनाएँ कर रहा था कि मैंने गणित के सारे सवाल हल कर लिए,किसी भी सवाल में अटका नहीं।
- दूसरा छात्र:कल्पना करना तो ठीक है पर उसे साकार भी तो करो,सवालों को हल करने का अभ्यास करो।
7.अयथार्थ कल्पनाएँ बनाम पुरुषार्थ (Frequently Asked Questions Related to Unrealistic Fantasies VS Manhood),कल्पनाओं का जाल बनाम पुरुषार्थ (Fantasy VS Manliness) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न:1.क्या कल्पनाएं अच्छी नहीं होती? (Aren’t fantasies good?):
उत्तर:भूत या प्रेत का जामा उन्हें धारण करना पड़ता है जो अपनी ही कल्पनाओं के गुलाम होते हैं।कल्पना मोहक और प्रिय प्रतीत होते हुए भी इसकी यथार्थ बातें सदा प्रिय नहीं होती।
प्रश्न:2.अच्छी कल्पनाएं किसके समान हैं? (What is good fantasy similar to?):
उत्तर:अच्छी कल्पना,सार्थक व व्यावहारिक कल्पना हमारी आत्मा का नेत्र है।
प्रश्न:3.पुरुषार्थ को स्पष्ट करें। (Clarify Purushartha?):
उत्तर:उन्नति के पथ पर आरोहण करने के इच्छुक,मानशाली धीर पुरुष आपत्ति-निवारण करने में समर्थ अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेना उचित मानते हैं।शूरवीरों का पुरुषार्थ ही सच्चा सहायक है।
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर द्वारा अयथार्थ कल्पनाएँ बनाम पुरुषार्थ (Unrealistic Fantasies VS Manhood),कल्पनाओं का जाल बनाम पुरुषार्थ (Fantasy VS Manliness) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| No. | Social Media | Url |
|---|---|---|
| 1. | click here | |
| 2. | you tube | click here |
| 3. | click here | |
| 4. | click here | |
| 5. | Facebook Page | click here |
| 6. | click here | |
| 7. | click here |