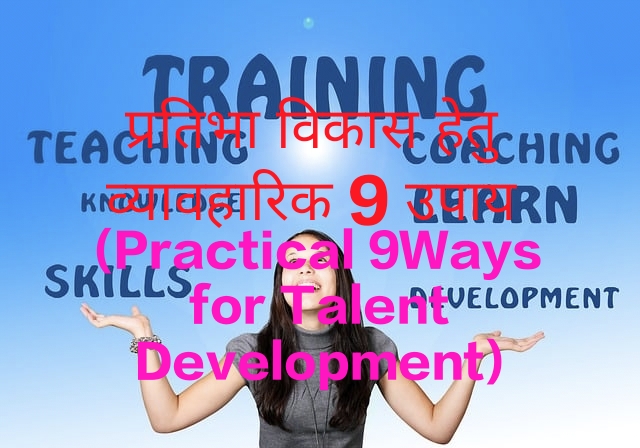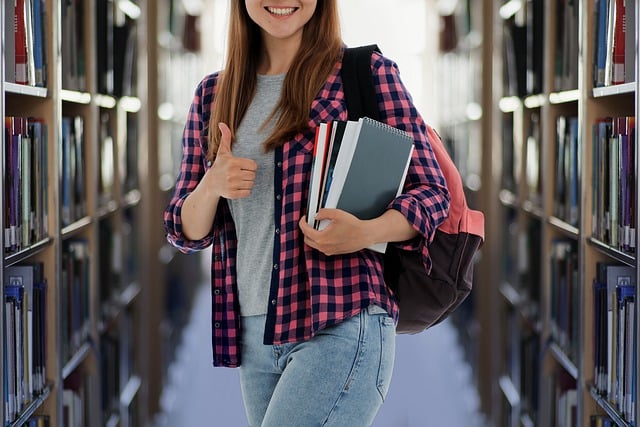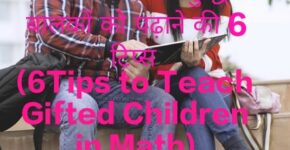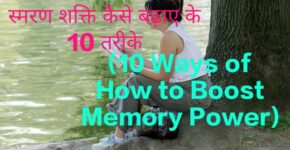Practical 9Ways for Talent Development
1.प्रतिभा विकास हेतु व्यावहारिक 9 उपाय (Practical 9Ways for Talent Development),छात्र-छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए 9 व्यावहारिक उपाय (9 Practical Ways for Talent Development of Students):
- प्रतिभा विकास हेतु व्यावहारिक 9 उपाय (Practical 9Ways for Talent Development) के आधार पर छात्र-छात्राएं जान सकेंगे कि प्रतिभा को कैसे तराशें? प्रतिभा का आशय सदैव लक्ष्योंन्मुख बुद्धि व भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए।ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न ही स्वयं को प्रेरणापुंज आदर्शों के प्रतीक रूप में उभारते एवं स्वयं को ही नहीं,अन्यों को भी निहाल करते हैं।
- बालकों को खेल-खेल में,गीत व कविता गाकर भी प्रतिभा संपादित करने की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है।अखाड़ों में निर्धारित अभ्यासों को अपनाना,शारीरिक अंगों को सशक्त बनाने के लिए व्यायामों का उपक्रम एवं आहार में परिवर्तन अभीष्ट माना जाता है।ऐसे ही कतिपय उपाय प्रतिभा को विकसित करने के लिए अपनाये जा सकते हैं और वे बहुत हद तक सफल हो सकते हैं यदि उन्हें उचित विधि और नियमों का पालन करते हुए किया जाए।
- आपको यह जानकारी रोचक व ज्ञानवर्धक लगे तो अपने मित्रों के साथ इस गणित के आर्टिकल को शेयर करें।यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो वेबसाइट को फॉलो करें और ईमेल सब्सक्रिप्शन को भी फॉलो करें।जिससे नए आर्टिकल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।यदि आर्टिकल पसन्द आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाईक करें जिससे वे भी लाभ उठाए।आपकी कोई समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Also Read This Article:5 Tip for Students to Develop Talent
2.ध्यान और योगासन करें (Do meditation and yoga):
- नियमित रूप से शौच,स्नानादि से निवृत्त होकर कुछ समय आज्ञा-चक्र में प्रकाशस्वरूप ॐ का या अपने इष्ट का ध्यान करें।इसे एकाग्रता सधती है।आपकी विभिन्न दिशाओं में बँटी हुई ऊर्जा एकाग्र होती है।अपनी मानसिक ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है तो प्रतिभा को विकसित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है।मनोबल कमजोर है,आपका चित्त चंचल है तो मन किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं होता है।एक विषय से दूसरे विषय पर फुदकता रहता है फलतः कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है।ध्यानावस्था की स्थिति आप अध्ययन करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं।अध्ययन को पूर्ण मनोयोग एवं रुचिपूर्वक करें,मन इधर-उधर भटके तो उसे अध्ययन पर फोकस करने का बार-बार अभ्यास करें।धीरे-धीरे अभ्यास करने से मन हर किसी काम पर एकाग्र होने लगेगा।यदि मन एकाग्र नहीं होगा तो कितना भी महान गुरु मिल जाए,कुछ भी साधना कर लें आपको कोई फायदा नहीं होगा।
- मन को एकाग्र करने में सबसे बड़ी बाधा आलस्य उत्पन्न करता है।अतः आलस्य को भगाने और शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए योगासन किया करें।यदि योगासन नहीं करना चाहें तो दो-तीन किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए।इससे शरीर में चुस्ती रहेगी,आलस्य नहीं आएगा,शरीर फिट रहेगा।योगासन करने के लिए किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लें।यदि कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो हल्के-फुल्के योगासन वीडियो और वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करके भी किए जा सकते हैं।इस साइट पर कुछ योगासनों के आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं उनसे भी आपको प्रेरणा मिल सकेगी।
- मन और शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा तो कोई भी योग साधना,जप,तप,पूजा-पाठ,अध्ययन-मनन-चिंतन आदि करना सरल हो जाएगा।मन को एकाग्र करना मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है।नियमित रूप से अभ्यास करने और धैर्य धारण करने से मन को वश में किया जा सकता है।एक बार मन को वश में करने के बाद भी उसको एकाग्र करने का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए।मन छूटे साँड की तरह है जो कभी इधर,कभी उधर,कभी यहाँ,कभी वहाँ दौड़ लगाता रहता है।ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मन को वश में करने का अभ्यास नहीं करते हैं।हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करने पर लगा रहता है जबकि मन को वश में करने के लिए आपको इस पर सतत निगरानी रखनी होगी और इस पर लगाम लगानी होगी।
3.आत्म-विश्लेषण और आत्म-सुधार (Self-Analysis and Self-Improvement):
- अपने आपका विश्लेषण करें,अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का निरीक्षण करें।अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का पता लगाना ही पर्याप्त नहीं है,पता लगाने के बाद उनमें सुधार करें।जो क्षमताएं हैं,योग्यता है उसमें और अधिक वृद्धि करें और जो कमजोरियां हैं उन्हें ढूंढ-ढूंढ कर,एक-एक करके निकाल फेंके।आत्म-विश्लेषण और आत्म-सुधार करना तभी संभव है जबकि आपको ज्ञान हो।बिना ज्ञान या अज्ञान के द्वारा आत्म-विश्लेषण करना संभव नहीं है।अतः रोजाना नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन,स्वाध्याय,सत्संग करें।
- आत्म-विश्लेषण न कर पाने का कारण यह भी है कि दरअसल हमारी नजर दूसरों पर पड़ती है खुद पर नहीं पड़ती इसलिए हम दूसरों को ही देखा करते हैं,खुद को नहीं देख पाते।हम दूसरों को ही जानते हैं,खुद को नहीं जान पाते।हम कोशिश भी यही करते हैं कि दूसरों को जानें-पहचानें,दूसरों से जान-पहचान बढ़ाएं पर न तो खुद को जानने की कोशिश करते हैं और न खुद से जान पहचान बढ़ाने की।इसीलिए हम आलोचना भी दूसरों की ही किया करते हैं खुद की आलोचना नहीं करते।दूसरों की आलोचना करने और उनकी गलतियां निकालने में हमें रस मिलता है क्योंकि इससे हमारा अहंकार बढ़ता है।हालांकि जो गलतियाँ हम दूसरों में खोजते हैं वे हम में भी हैं पर उन पर हमारी नजर नहीं पड़ती।यदि हम अपनी गलतियों पर ध्यान दें,आत्म-निरीक्षण किया करें तो हमें दूसरों की गलतियों को देखने का समय ही नहीं मिले।पर आत्म-विश्लेषण के साथ आत्म-सुधार करना भी आवश्यक है।
4.स्वसंकेत (Autosuggestion):
- इसकी विधि यह है कि चटाई,दरी या मेट पर शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन बैठा जाए। भावना की जाए कि मेरे समस्त शरीर में,प्रत्येक अंग अवयवों में चेतना ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।शिथिलता,निष्क्रियता शरीर से निकल रही है और उसके स्थान पर सक्रियता शरीर ग्रहण कर रहा है।शरीर का प्रत्येक अंग पुष्ट और सुगठित हो रहा है।इंद्रियों की क्षमता में वृद्धि हो रही है।चेहरे पर चमक बढ़ रही है।बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है,जिसका अनुभव प्रतिभा विकास के रूप में अपने को तथा दूसरों को हो सके।
- वस्तुतः स्वसंकेतों में मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है।जो जैसा सोचता है और अपने संबंध में भावना करता है,वह वैसा ही बन जाता है।विधेयात्मक चिंतन से हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है और अवगुणों का निष्कासन होता है।जबकि नकारात्मक चिंतन से हमारे गुणों का ह्रास होता है और अवगुणों की वृद्धि होती जाती है।महापुरुषों,महान गणितज्ञों और महान वैज्ञानिकों के गुणों का चिंतन करेंगे तो वैसे ही गुण हमारे अंदर खिंचते चले आते हैं और प्रभावोत्पादक परिणाम देखने को मिलते हैं।
- एक प्रकार से स्व-संकेतों द्वारा अपने आभामंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है।मनोवैज्ञानिक कहते हैं-“थिंक एंड ग्रो रिच” अथवा “अडॉप्ट पॉजिटिव टुडे”।आशय यह है कि सोचिए,विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए,ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें।सारे महामानव स्व-संकेतों से ही महान बन सके हैं।उन महान गणितज्ञों और वैज्ञानिकों की जीवनी देखिए और उनके कार्यों का विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने महान् खोजें कैसे कर दी।उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में चिंतन की बहुत बड़ी भूमिका थी।आप भी स्वसंकेतों का प्रयोग करके देखिए आपको आगे बढ़ने की कुंजी मिल जाएगी,गुत्थियां सुलझ जाएंगी।
5.सूर्यभेदी प्राणायाम (Suryabhedi Pranayama):
- स्नानादि से निवृत्त होकर मेट पर ध्यान मुद्रा में बैठा जाए।कपड़े शरीर पर कम से कम हों।मुख सूर्य की ओर हो,समय प्रातःकाल का।अपने अभ्यस्त आसन से पूर्ववत बैठकर सूर्यनाड़ी (दायें नथुने) से धीरे-धीरे शब्द करते हुए प्राण का पूरक करें,(प्राणवायु को कण्ठ,हृदय और पेट में भली प्रकार भर कर) यथाशक्ति कुंभक करें-इसमें ऐसी प्रतीति होनी चाहिए कि शिखा से लेकर पाद-नख पर्यंत प्राणवायु देह में भर गया है।जब कुछ घबराहट सी होने लगे तब दाएं नासाछिद्र को दबाकर चंद्रनाड़ी (बाएँ नथुने) से शब्द करते हुए वेगपूर्वक रेचन कर दें।इस प्राणायाम में पुन:-पुनः सूर्यनाड़ी से पूरक और चंद्रनाड़ी से रेचक किया जाता है।प्रथम दिन तीन प्राणायाम करें और फिर एक-दो दिन के पीछे एक-एक बढ़ाते चलें,बलाबल के अनुसार 21 तक बढ़ाया जा सकता है।इस प्राणायाम को प्रायः शीतकाल में करना चाहिए।
- प्राणायाम करते समय भावना करें कि सूर्य ऊर्जा से अपनी चेतना भर रही है।दायीं नासिका से खींचा श्वास अंदर तक जाकर सूर्यचक्र को आंदोलन उत्तेजित कर रहा है।वापस बायीं नासिका से सारे दुर्गुण निकल रहे हैं।पहले की अपेक्षा अब अपने में प्राण ऊर्जा की मात्रा भी अधिक बढ़ गई है,जो प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अनुभव में आती है।क्रिया को गौण व भावना को प्रधान मानते हुए यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए,तो निश्चित ही फलदायी होता है।
6.पणवध्वन्यात्मक प्राणायाम (Pranavadhvanyatmak Pranayama):
- कमर सीधी,कमलासन में हाथ गोदी में,मेरुदंड सीधा रखकर बैठ जाए।पूरक द्वारा मूलाधार तक प्राणवायु को भर दें।तत्पश्चात ओष्ठों को थोड़ा-सा खोलकर ओम (ॐ) की गुंजायमान सुरीली मधुर झंकार युक्त लंबे प्रश्वास को एकतानतापूर्वक धीरे-धीरे रेचन करें;मुख से होती हुई इस ध्वनि में निमग्न होकर नेत्र बंद कर लें।नित्यप्रति इस ध्वनि को सुनते हुए प्राणायाम की संख्या में वृद्धि करते जाएं।ध्वनि-पूर्वक जप के साथ प्राणायाम में ऐसा नियम रहता है कि 40 सेकंड तक ‘ओ’ तथा 20 सेकंड तक ‘म’ की ध्वनि की जाती है।इसी काल-क्रम से प्राणायाम में वृद्धि करते जाएं।
- लाभ:श्वास-प्रश्वास का दीर्घ तथा सूक्ष्म होना,मन का शांत,बुद्धि और चित्त का स्थिर होना,अध्ययन के प्रति अगाध श्रद्धा की प्रबलता तथा दुर्गुणों को निकालना (वैराग्य),प्रणव-जप में निमग्नता का होना,वाणी में मधुरता आना,ध्यान की स्थिरता आदि लाभ होते हैं।इसके निरन्तर अभ्यास से ‘प्रणव ध्वनि’ स्वतः होकर दिन-रात बनी रहती है।इनमें निमग्न होकर और निश्छल होकर मन समाधि में सहायक बनता है।
7.महापुरुषों के साथ सत्संग (Satsang with great men):
- महान् गणितज्ञों और महान् वैज्ञानिकों का निकट संपर्क संभव हो तो कुछ समय उनके सानिध्य में,उनकी छत्रछाया में रहना चाहिए और उनकी अमृतवाणी का रसास्वादन करना चाहिए।महापुरुष,महान् गणितज्ञ और महान वैज्ञानिक निष्कपट,निश्चल,सरल हृदय होते हैं,अतः ऐसे व्यक्तियों के हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है।कहा भी गया है कि ‘बिनु सत्संग विवेक न होई’ अर्थात् सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता है।यह सत्संग महान् लोगों,वरिष्ठों,सज्जनों,ज्ञानियों आदि के साथ ही होना चाहिए।उनकी आभा का तेज हमारी ओर प्रवाहित होता है और हम उनके निकट सानिध्य से अपने गुणों में वृद्धि ही करते हैं।जैसे पारस के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है।निर्मली के बीज से मटमैला पानी स्वच्छ हो जाता है वैसे ही विद्वानों,ज्ञानियों,सज्जनों आदि की संगति से मूर्ख भी विद्वान,सज्जन,प्रतिभावान बन जाता है।सत्संग से हमारा एक-एक गुण खिल उठता है।
8.नाद योग (Naad Yoga):
- वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने-अपने प्रभाव है।उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा परिवर्धन में सहायक होता है।यह कार्य,शब्द शक्ति (जो चेतना का इंधन है) के श्रवण से अंतः के ऊर्जा केन्द्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव है। टेपरिकॉर्ड से भजन व संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है,आजकल तो इंटरनेट मोबाइल से भी यह कार्य संभव है एवं उच्चारित मन्त्रों या संगीत अथवा भजन पर ध्यान लगाकर भी।अपने लिए उपयुक्त भजन,मंत्र या संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए।एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए।यह श्रवण 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए।क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है।इस विषय पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए धुनों का चयन कर सुनने का कार्य संपन्न होता है।
9.प्रायश्चित (atonement):
- व्यभिचार,छल,धन अपहरण,कपट,झूठ बोलना,लोभ,लालच आदि जैसे दुष्कर्मों से भी प्राणशक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है।इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएँ।व्रत-उपवास,दान-पुण्य चान्द्रायण जैसे व्रत उपवास भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं।कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे,इसके लिए अपने गुरु,शिक्षक,वरिष्ठजन जैसे विशेषज्ञों से अपनी बात कह कर काफी हल्कापन आ जाता है व आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है।प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है।प्रतिभा संवर्द्धन हेतु अंतरंग की धुलाई करनी जरूरी भी है।
10.छात्र-छात्राएं सही लक्ष्य निर्धारण करें (Students should set the right goals):
- गलत लक्ष्य पर चलने वाला वहां जा पहुंचता है जहां उसे जाना न था और वहां नहीं पहुंच पाता जहाँ उसे जाना था।इसे भटकना कहते हैं जो हमारा समय और श्रम तो नष्ट करता ही है साथ ही कई हानियां भी करता है लिहाजा अगर गलत लक्ष्य पर चलते हुए किसी छात्र-छात्रा को यह समझ आ जाए या कोई उसे समझा दे कि वह गलत लक्ष्य पर चल रहा है तो उसे उसी वक़्त आगे बढ़ना बंद करके सही लक्ष्य का चुनाव कर लेना चाहिए।सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता।जब नींद खुले तभी सवेरा मानकर उठ जाना चाहिए।इस पहली बात को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन,लक्ष्य की दिशा और दशा ठीक करने में देर नहीं करना चाहिए।
- दूसरी बात यात्रा वही सफल मानी जाती है जो हमें हमारे सही लक्ष्य तक पहुंचा दे;हमारे अभीष्ट लक्ष्य को उपलब्ध करा दे और हमारे श्रम,समय और व्यय को सार्थक कर दे।यदि ऐसा नहीं हो पाए तो वह यात्रा,यात्रा नहीं,भटकना ही हुआ,पथभ्रष्ट होना हुआ।अच्छा काम वही होता है जिसका आरंभ अच्चे विचार और श्रेष्ठ उद्देश्य से हुआ हो और जिसका अंत अच्छा हो।जो कार्य शुरू में या मध्य में मजा दे पर जिसका अंत दुखदायी,कष्टकारी,अनर्थकारी हो,वह अच्छा कैसे हो सकता है? कुकर्म उसी को तो कहा जाता है जो कुफल देता है और सुफल से वंचित रखता है।
- आज अधिकांश छात्र-छात्राएं जिस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं,किसी भी रूप में,किसी भी स्तर पर जो यात्रा की जा रही है क्या इसकी दिशा ठीक है? क्या हमारी प्रतिभा को विकसित करने की तरफ हो रही है? क्या हमारी राह और मंजिल ठीक है? इन सभी सवालों पर गौर करते हुए अपनी व्यक्तिगत यात्रा,लक्ष्य के विषय पर भी विचार करें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे की वह कहां जा रहा है,उसका लक्ष्य सही है या नहीं,उसकी प्रतिभा का विकास हो रहा है या नहीं।इन पर विचार-मनन-चिंतन और गौर करें।
- उपर्युक्त आर्टिकल में प्रतिभा विकास हेतु व्यावहारिक 9 उपाय (Practical 9Ways for Talent Development),छात्र-छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए 9 व्यावहारिक उपाय (9 Practical Ways for Talent Development of Students) के बारे में बताया गया है।
Also Read This Article:4 Top Tips to Become Strong Person
11.प्रतिभा विकास का जमाना (हास्य-व्यंग्य) (Age of Talent Development) (Humour-Satire):
- पिता:बेटा एक जमाना था जब प्रतिभा विकसित करने वाले केन्द्रों की फीस सिर्फ 10-20 रुपए हुआ करती थी।
- पुत्र:अब संभव नहीं है।क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,वाईफाई इंटरनेट मिलता है,संगीत की धुने चलती रहती हैं,बिल्डिंग आलीशान और हर साधन-सुविधाओं से सुसज्जित है।
- पिता:लेकिन तुझे देखकर कह सकता हूं की प्रतिभा विकास के नाम पर जीरो प्रोग्रेस है।
12.प्रतिभा विकास हेतु व्यावहारिक 9 उपाय (Frequently Asked Questions Related to Practical 9Ways for Talent Development),छात्र-छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए 9 व्यावहारिक उपाय (9 Practical Ways for Talent Development of Students) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न:1.जीवन कब खिलता है? (When does life bloom?):
उत्तर:जीवन का सौंदर्य तभी निखरता है,खिलता है,जब साहस और संकल्प बल के आधार पर विकास मार्ग पर आने वाले अवरोधों से जूझते हुए चला जाए।ऐसे व्यक्तिवान दृढ़संकल्पी ही अपना और देश का कुछ हित साधन कर पाए हैं।
प्रश्न:2.प्रतिभावान आगे कैसे बढ़ाते हैं? (How do the talents move forward?):
उत्तर:प्रतिभावान अंधकार से जूझकर प्रकाश फैलाते हैं। मनोयोग एवं प्रखरता के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना संभव नहीं है।प्रगतिशीलों के लिए एक ही संदेश है:तप और साधना कर।
प्रश्न:3.प्रतिभा से क्या आशय है? (What do you mean by talent?):
उत्तर:प्रतिभा का वास्तविक आशय बौद्धिक विकास से न होकर आंतरिक विकास से संबंधित है।अंतः प्रेरणा प्रतिभा का मुख्य स्रोत है।जो विशेषता प्रयत्नपूर्वक उभारी जाती है,उसे प्रतिभा कहते हैं।
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर द्वारा प्रतिभा विकास हेतु व्यावहारिक 9 उपाय (Practical 9Ways for Talent Development),छात्र-छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए 9 व्यावहारिक उपाय (9 Practical Ways for Talent Development of Students) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| No. | Social Media | Url |
|---|---|---|
| 1. | click here | |
| 2. | you tube | click here |
| 3. | click here | |
| 4. | click here | |
| 5. | Facebook Page | click here |
| 6. | click here | |
| 7. | click here |
Related Posts
About Author
Satyam
About my self I am owner of Mathematics Satyam website.I am satya narain kumawat from manoharpur district-jaipur (Rajasthan) India pin code-303104.My qualification -B.SC. B.ed. I have read about m.sc. books,psychology,philosophy,spiritual, vedic,religious,yoga,health and different many knowledgeable books.I have about 15 years teaching experience upto M.sc. ,M.com.,English and science.